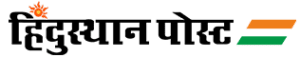विजय सिंगल
Bhagavad Gita:आनंद अर्थात सुख मानव जीवन का सार्वभौमिक लक्ष्य है। आरंभ से ही मनुष्य आनंद की खोज में है। लेकिन उसके लिए प्रायः: यह मृग मरीचिका ही साबित हुआ है। जितना ही वह उसके पीछे भागता है, उतना ही वह उसे चकमा देता है। भगवत गीता ने सुख के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और व्यापक कल्याण का एक स्पष्ट संदेश दिया है। श्रीकृष्ण ने अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही बल देकर कहा है कि शोक का कोई कारण नहीं है; क्योंकि आत्मा, व्यक्ति की मूल प्रकृति, अमर है और किसी भी दुख से परे है।
तीन प्रकार के सुख
भौतिक प्रकृति के तीन भेदों( गुणों) के अनुरूप सुख भी तीन प्रकार के कह गए हैं श्लोक संख्या (18.36 से 18.39) आत्मा की स्पष्ट समझ से जो सुख उत्पन्न होता है, उसे अच्छाई के गुण वाला ( सात्विक सुख) कहा गया है। इस प्रकार का आनंद, जिसके परिणाम स्वरूप सभी दुखों का अंत हो जाता है, लंबे आध्यात्मिक अभ्यास के पश्चात प्राप्त होता है। यद्यपि शुरू में यह जहर की भांति प्रतीत होता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत की तरह होता है। इंद्रियों के, उनके विषयों के साथ होने वाले संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है, उसे रजोगुण (राजसिक सुख) माना जाता है । ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन इसका परिणाम विष के समान होता है। और जो आदि से अंत तक आत्मा को भरमाता है; तथा जो निद्रा, आलस्य और लापरवाही के कारण उत्पन्न होता है-ऐसा सुख तमोगुणी (तामसिक सुख )कहलाता है।
इस तरह, सुख का प्रकार, गुणों के अनुसार बदलता रहता है। इन्द्रियों की तृप्ति से होने वाला सुख तामसिक सुख कहलाता है। ऐसे क्षणिक सुख व्यक्ति को प्रमाद में धकेल देते हैं और आत्मा को अज्ञान के अंधकार से ढक देते हैं। ऐसे सुखों में आसक्त तामसिक व्यक्ति जीवन भर अपने को कुकर्मों से बंधा रहता है।
एक राजसिक व्यक्ति को अपने धन, सत्ता तथा कीर्ति से सुख का आभास होता है। ऐसा सुख शुरू में बहुत आकर्षक और सुखद लगता है क्योंकि यह विलास तथा स्वामित्व का गर्व देता है; लेकिन अंत में यह कष्ट का ही कारण सिद्ध होता है क्योंकि यह ऐसी नई-नई इच्छाओं को जन्म देता है, जिनका कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि आज के सुख में कल के दुख का बीज छिपा रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक सुख अल्पकालिक है। इसलिए सांसारिक भोगों के क्षेत्र में व्यक्तियों को अति भोग से बचना चाहिए।
अपने ही भीतर सुख
आध्यात्मिक अभ्यास प्रारंभ में तो कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि यह बहुत संयम और अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अंतत वे सांसारिक दुखों के पार पहुंचा देते हैं सात्विक सुख व्यक्ति के अपने ही मन की शांति से उत्पन्न होता है, जब कोई मनुष्य भौतिक सुखों की चिंता करना छोड़ देता है तो वह सुख को अपने ही भीतर पाता है, एक ऐसा आनंद जो स्वयं उसकी आत्मा में स्थित है। ऐसा आंतरिक सुख दीर्घकालीन होता है क्योंकि यह किसी ब्रह्म कारक जैसे किसी वस्तु, जीव या स्थिति पर निर्भर नहीं होता। ऐसा प्रसनचित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अविचलित रहता है तथा बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता।
तीनों सुखों का अपना-अपना महत्व
उक्त तीनों प्रकार के सुख परस्पर अनन्य नहीं है। तीनों सुखों का अपना -अपना महत्व है। वस्तुत:, यह सब मिलकर ही जीवन को सुखद बनाते हैं। यह बात जरूर कहीं जा सकती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इन सुखों में से किसी एक का प्रभुत्व होना उसे व्यक्ति के सुख की समग्र गुणवत्ता को निर्धारित करता है।
आनंद की ओर ले जाने वाले दो मार्ग
मोटे तौर पर कहे तो दो ही ऐसे मार्ग हैं जो आनंद की ओर ले जाते हैं- पहला ‘ सुगम लेकिन हानिकारक” तथा दूसरा” दुर्गम लेकिन हितकारी” यह क्रमशः अल्पकालीन और चिरकालिक सुख के मार्ग हैं। भारी सुखों की चकाचौंध से आकर्षित होने वाले अज्ञानीजन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनैतिक व्यवहार का मार्ग चुनते हैं और अंततः दुख भोगते हैं ।लेकिन ज्ञानीजन भौतिक जगत के लुभावनेपन के बहकावे में नहीं आते तथा अनन्य भक्ति और अनासक्त कर्म के सही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह ज्ञानीजन दीर्घकालीन आनंद को प्राप्त करते हैं।
खुशी को बढ़ाने वाले गुण
भगवत गीता ने उन मानवीय गुणों की भी गणना की है, जो खुशी को बढ़ावा देते हैं। सच्चे सुख के लिए मन की शांति पहली शर्त है, बिना शांत मन के कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। आगे कहा गया है कि वास्तविक शांति केवल वही प्राप्त कर सकता है, जो वासनाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, जो लालसा से मुक्त है, जिसमें “मेरेपन” का भाव नहीं है; तथा जो मिथ्या अहंकार से रहित है। ऐसा शांत व्यक्ति ही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है।इच्छाओं के गुलाम ना तो शांति प्राप्त कर सकते हैं और ना ही सुख। उस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति को स्वयं में संतुष्ट होने और परमात्मा के साथ एकाकार होकर रहने से प्राप्त होता है।
मन का संतुलित होना आवश्यक
मन का समभाव आनंदमय जीवन का एक अनिवार्य अंग है। व्यक्ति को पूर्ण समचित्तता का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए तथा मार्ग में जो भी आए, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जिन बुद्धिमान पुरुषों का मन संतुलित होता है और जिन्होंने अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, वह उसे आनंद में अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो किसी भी दुख से परे है। जो काम और क्रोध के आवेगों को झेलने में सक्षम है, वही सुखी हो सकता है। सर्वोच्च सुख उसी को मिल पाता है जिसका मन शांत है, जो बुराई से मुक्त है, जिसका जुनून शांत है, जो पाप के लेशमात्र से भी मुक्त है; और जिसका मन आत्मा में लगा रहता है। यह भी कहा गया है की प्रसन्नता उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिनकी आस्था अटल है और जो संशय वृत्ति का नहीं है।
निष्कर्ष:
व्यक्ति की सुख के खोज की यात्रा, बाहरी यात्रा से अधिक एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। सच्चा आनंद वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जिसका मन स्थिर, सम और निर्मल है; और जिसकी आत्मा शुद्ध है। जब कोई मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह संतोष प्राप्त करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। वह ना तो दुख से व्याकुल होता है और न सुख की लालसा रखता है। वह बस खुश है, संतुष्ट है।